हमारे संस्थापक पिता और ग्रामीण जीवन पर उनके परस्पर विरोधी विचार
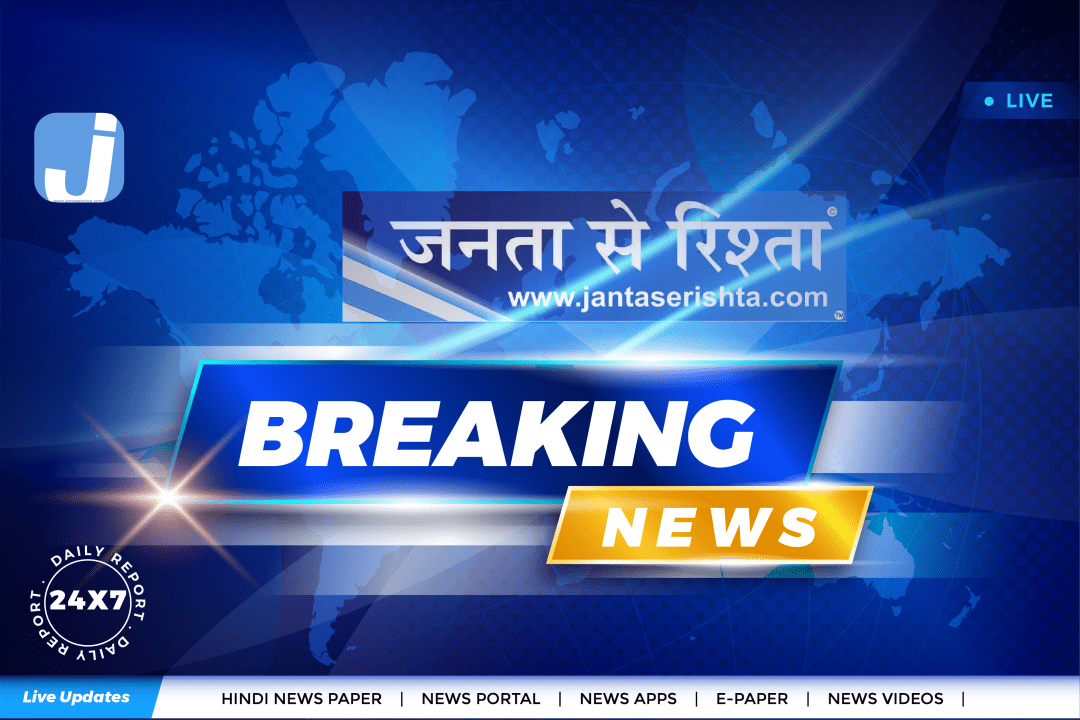
शायद ही कोई ऐसी किताब आती हो जिसे न केवल विषय विशेषज्ञों के नजरिए से, बल्कि आम लोगों के नजरिए से भी पढ़ने और समझने की जरूरत हो ताकि ग्रामीण और शहरी भारत के बीच संबंधों को समझा और पहचाना जा सके।

प्रोफेसर सुरिंदर एस. जोडखा की ‘द इंडियन विलेज: रूरल लाइव्स इन द 21 सेंचुरी’ (अलेफ बुक्स; 799 रुपये) इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे स्वतंत्र भारत के संस्थापकों ने संतुलन को सही करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन बहुत अलग एजेंडे को आगे बढ़ाया। .प्रो. जोडखा ने पाठक को यह समझाने के लिए धर्म, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता की बुराई के मुद्दों पर चर्चा की कि स्वतंत्रता के बाद ‘ग्राम गणराज्य’ का विचार कैसे विकसित हुआ। लेखक ने प्रामाणिक रूप से किसानों के जीवन, भारतीय गांवों के बारे में ब्रिटिश दृष्टिकोण, 1947 के बाद ग्रामीण समाज और कृषि पद्धतियों को कैसे नया रूप दिया गया, के बारे में विस्तार से बताया है।
पुस्तक में असली बात अध्याय 3 है जहां प्रो. जोडखा तीन प्रभावशाली विचारकों – महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बी.आर. के कार्यों का विश्लेषण करते हैं। अम्बेडकर–जिनके गाँवों के बारे में विचार स्वतंत्र और स्वतंत्र भारत के उनके दृष्टिकोण को भी दर्शाते हैं।
भारतीय गाँवों के बारे में उनका दृष्टिकोण औपनिवेशिक शक्तियों का मुकाबला करने के लिए की गई महज राजनीतिक बयानबाजी नहीं थी। इन विचारकों में सबसे महत्वपूर्ण थे महात्मा गांधी, जिनके ग्रामीण समाज के बारे में विचार सर्वविदित हैं।
गांधी ने ज़ोर देकर कहा था: “मेरे लिए, भारत गांवों में शुरू और समाप्त होता है।” वे जीवन भर अपनी रचनाओं में ग्राम्य जीवन के मूल्य को भी रेखांकित करते रहे। वह “गाँव भारत की आत्मा हैं” के विचार के सबसे प्रबल और प्रेरक समर्थक थे।
प्रो. जोडखा का कहना है कि गांधी द्वारा भारतीय गांव के विचार का आह्वान दक्षिण अफ्रीका में उनके दिनों के दौरान विकसित हुआ प्रतीत होता है। गांधी ने ग्रामीण जीवन को जीवन जीने के एक वैकल्पिक तरीके, एक आदर्शलोक के रूप में देखना जारी रखा, तब भी जब उन्हें भारतीय ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं में खामियां नजर आईं।
उन्होंने गांव नहीं छोड़ा बल्कि वहां की राजनीति को उलट-पुलट कर दिया। उनका मानना था कि वास्तविक स्व-शासन या स्वराज केवल भारत की सभ्यतागत ताकत को बहाल करके ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसका अर्थ है इसके ग्राम समुदायों का पुनरुद्धार।
लेखक का कहना है कि गांधी की ग्रामीण जीवन की वकालत परंपरावाद का जश्न मनाने के लिए नहीं थी; उनकी अपील एक प्रकार की समानता की थी जिसके तहत गाँवों को एक निम्न स्थान के रूप में न समझा जाए। गांधीजी का मानना था कि अगर भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरना है तो गांव स्वायत्तता के हकदार हैं।
गांधी के भरोसेमंद शिष्य नेहरू, स्वतंत्र भारत में स्वायत्त गांव की प्रधानता के मुद्दे पर अपने गुरु से असहमत थे। उन्होंने पारंपरिक सामाजिक संरचना की समीक्षा करने में कोई गुण नहीं देखा, क्योंकि औपनिवेशिक और प्राच्यवादी लेखन ने संभवतः इसकी कल्पना या निर्माण किया था।
नेहरू के लिए, जाति की समस्या का समाधान लोकतांत्रिक और आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की ओर आगे बढ़ना था। उन्हें भारतीय किसानों के राजनीतिक रूप से विनम्र और भाग्यवादी स्वभाव पर भी निराशा हुई, उनका मानना था कि उनमें अकाल, बाढ़, बीमारी और भीषण गरीबी को सहन करने की क्षमता है, और जब वे इन कष्टों को सहन नहीं कर सकते, तो वे चुपचाप लेट जाते हैं और मर जाते हैं। यही उनका भागने का रास्ता था.
अम्बेडकर गांधी और नेहरू दोनों के दर्शन के प्रतिद्वंद्वी थे। प्रो. जोधका का कहना है कि अम्बेडकर ग्रामीण जीवन पर गांधी और नेहरू दोनों के विचारों के आलोचक थे और वे कैसे स्वतंत्र भारत को आगे ले जाना चाहते थे।
अम्बेडकर के अनुसार गाँव, “हिन्दू सामाजिक व्यवस्था का कार्यकारी संयंत्र” था जहाँ कोई भी “हिन्दू सामाजिक व्यवस्था को पूरे जोरों पर चल रहा हुआ” देख सकता था। एक सामंजस्यपूर्ण समुदाय होने से दूर, अम्बेडकर के लिए गाँव दमनकारी जाति व्यवस्था की नींव पर टिका हुआ एक विभाजित ब्रह्मांड था।
प्रो. जोडखा कहते हैं कि अंबेडकर के कुछ तर्क संविधान सभा की बहस के दौरान सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट हुए थे, जहां कुछ सदस्यों ने गांव को अपनी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ एक स्वायत्त प्रशासनिक इकाई बनाने के लिए उत्साहपूर्वक तर्क दिया था।
अम्बेडकर ने इस तरह के कदम का पुरजोर विरोध किया था। दूसरी ओर, गांधी और नेहरू ने ‘ग्राम समुदाय’ की औपनिवेशिक संरचना को भारत के अतीत की वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया था। अम्बेडकर ने इसे अधिक गंभीरता से देखा। सामाजिक विज्ञान में अम्बेडकर के प्रशिक्षण को देखते हुए, वह भारत के प्राच्यवादी आख्यान में इस निर्माण के स्रोतों का पता लगाने में सक्षम थे।
उन्होंने भारत के मध्यवर्गीय अभिजात्य वर्ग द्वारा इसकी आलोचना रहित स्वीकृति के लिए एक समाजशास्त्रीय स्पष्टीकरण भी प्रदान किया। गाँव के प्रति उनके मन में कोई विशेष सम्मान नहीं था। गाँवों की जमीनी हकीकतों को वे अच्छी तरह समझते थे और भारतीय समाज की अलोकतांत्रिक भावना की उनकी आलोचना का स्रोत बने।
लेखक का कहना है कि अम्बेडकर के लिए गाँव हिंदू सामाजिक व्यवस्था का एक सूक्ष्म रूप था, जो जाति के पदानुक्रम और बहिष्कार और भेदभाव की संस्कृति से चिह्नित था, जो ग्रामीण बस्ती के भीतर जाति-आधारित स्थानिक विभाजन में सबसे अच्छी तरह से परिलक्षित होता था।

















