स्टील फ्रेम को अपूरणीय क्षति का खतरा है
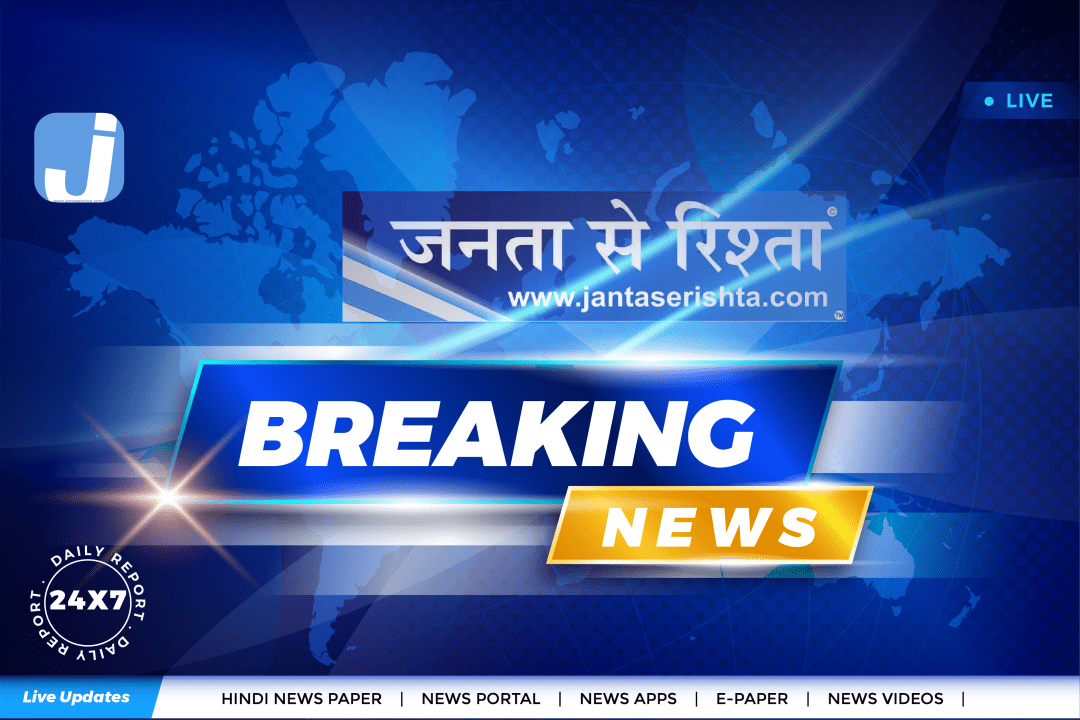
देश की सिविल सेवा, जिसे अक्सर स्टील फ्रेम के रूप में जाना जाता है, ने पिछले सात दशकों में कई राजनीतिक उथल-पुथल और अनिश्चितताओं को सहन किया है। यद्यपि अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं ने हमारे विविध राजनीतिक इतिहास के दौरान चुनौतियों का सामना करने के बावजूद हमेशा अपनी चरम क्षमता पर प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने सहनीय रूप से अच्छा प्रबंधन किया है। हमारी नौकरशाही स्थायी है क्योंकि हर आने वाली सरकार आधिकारिक तंत्र को चलाने के लिए अपने लोगों को शामिल नहीं करती है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि सभी स्तरों पर सरकारी कर्मचारी भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं। वे सत्ता में पार्टी की राजनीति और नीतियों की परवाह किए बिना चुनी हुई सरकारों के आदेशों और निर्णयों को पूरा करते हैं।

जब तक सत्ता में बैठे लोग नौकरशाही की स्वतंत्रता की सराहना करते हैं और इसका उपयोग वैध विकास और प्रवर्तन के लिए करते हैं, तब तक यह व्यवस्था एकदम सही है। हालाँकि, मानवीय कमज़ोरियाँ ऐसी सैद्धांतिक रूप से परिपूर्ण व्यवस्थाओं को बाधित करने के लिए बाध्य हैं। यह पहली बार प्रधान मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान स्पष्ट हुआ जब उन्होंने ‘प्रतिबद्ध सिविल सेवा’ के गुणों की प्रशंसा की। उन्होंने शायद प्रतिबद्धता को विकास और लोगों के हितों के प्रति समर्पण के रूप में तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। लेकिन नौकरशाही ने ‘प्रतिबद्ध सिविल सेवा’ के आह्वान को पार्टी और सत्ता में बैठे नेता के प्रति वफादारी की मांग के रूप में पढ़ा।
नौकरशाही में प्रतिबद्धता इंदिरा गांधी से पहले सेवा संगठनों के रूप में रही है, जिन्होंने कई राज्यों में और केंद्र में प्रमुख संगठनों में कर्मचारियों को राजनीतिक आधार पर अलग कर दिया था। ऐसी पक्षपातपूर्ण निष्ठाओं पर आरोपित, प्रतिबद्ध सिविल सेवा अवधारणा ने ‘भरोसेमंद और वफादार अधिकारी’ और ‘हमारे साथ नहीं’ प्रकार के लोगों का निर्माण करके नौकरशाही के उच्च क्षेत्रों में दरारें पैदा कीं। एक बार जब विश्वसनीय अधिकारियों को शानदार पोस्टिंग, आकर्षक भत्ते और संवैधानिक पदों पर पदोन्नति जैसे वफादारी का पुरस्कार मिलता हुआ देखा जाता है, और ‘हमारे साथ नहीं’ और स्वतंत्र अधिकारियों को नजरअंदाज, परेशान और दंडित किया जाता है, तो संदेश स्पष्ट और स्पष्ट हो जाता है। .
क्रेडिट: new indian express

















