सावधानीपूर्वक जांच
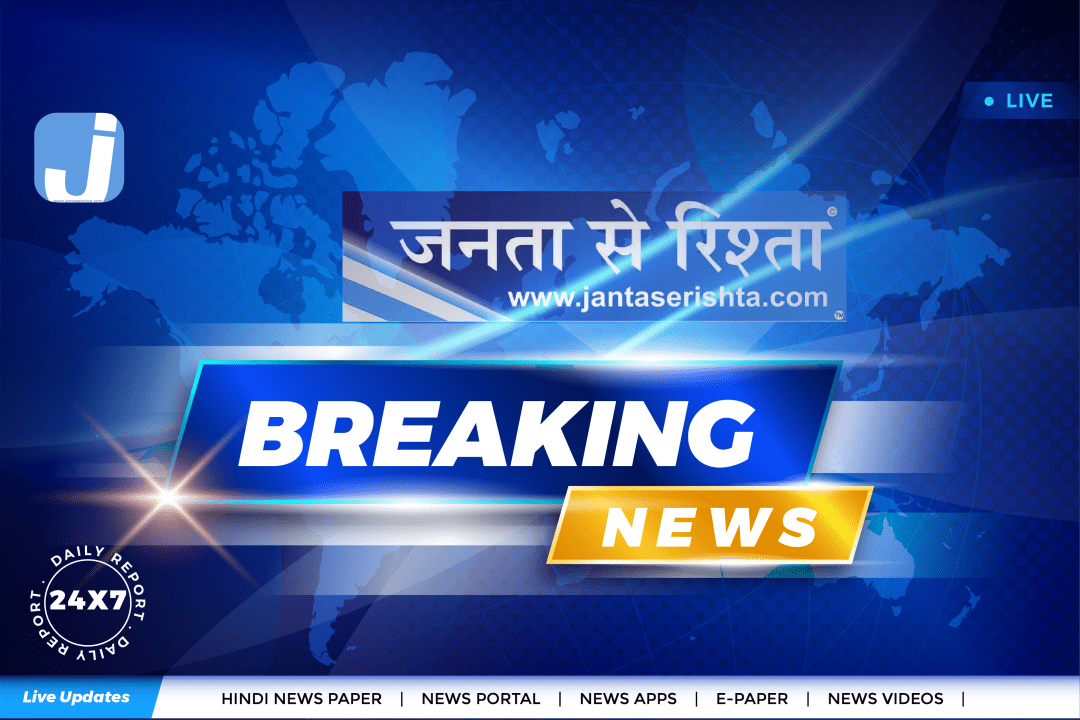
आम चुनाव की पूर्व संध्या पर ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का मुद्दा एक बार फिर गर्म है। राजनीतिक समुदाय और मीडिया के एक वर्ग के लिए यह समय की मांग है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 29 जनवरी, 2018 को संसद में अपने संबोधन में राष्ट्रीय और मानव संसाधनों पर लगातार चुनावों के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में तर्क दिया। प्रधान मंत्री ने 2019 में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी इसी विचार को जोरदार ढंग से दोहराया। केंद्र सरकार ने अब एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक पैनल का गठन किया है।

चुनाव अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के इंजन हैं। इन्हें एक बार में दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में माना जा सकता है क्योंकि वे मतदाताओं को न केवल अपने नेताओं को चुनने में सक्षम बनाते हैं बल्कि उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित करते हैं। चुनाव जनता की राय की अभिव्यक्ति को सुविधाजनक बनाते हैं और शासन करने की वैधता सुनिश्चित करते हैं।
भारत में 1967 तक एक साथ चुनाव होते रहे थे। 1968-69 में कुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने और 1970 में चुनावों से पहले लोकसभा के निलंबन से एक झटका लगा क्योंकि संसदीय और राज्य चुनाव चक्र दलबदल जैसे कारकों के कारण असंतुलित हो गया। , 1967 से विभाजन और विघटन।
लोकतंत्र में एक साथ चुनाव अज्ञात नहीं हैं। उदाहरण के लिए, स्वीडन में, राष्ट्रीय विधायिका, प्रांतीय विधायिका और काउंटी परिषदों के चुनाव न केवल एक साथ होते हैं, बल्कि एक निश्चित दिन पर भी होते हैं – हर चार साल में सितंबर का दूसरा रविवार। दक्षिण अफ़्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं के चुनाव पाँच साल के अंतराल पर होते हैं। नेपाल में 2017 में राष्ट्रीय और राज्य चुनाव एक साथ हुए थे। कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 79वीं रिपोर्ट में 2015 में एक साथ चुनाव कराने की वकालत की थी। इसका ब्लू प्रिंट भी तैयार किया गया।
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का फॉर्मूला समझदारी भरा लगता है और इसके कुछ अंतर्निहित फायदे भी हैं क्योंकि यह सभी स्तरों पर लोकतांत्रिक संरचनाओं को बिना किसी रुकावट के विकास और शासन पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। आचार संहिता लागू होने से अक्सर महत्वपूर्ण और जरूरी नीतिगत निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न होती है।
हमारे जैसे बड़े देश में चुनाव बेहद महंगी और समय लेने वाली प्रक्रिया है। इस तथ्य को देखते हुए कि राजनीतिक दलों को विभिन्न स्रोतों से धन जुटाना पड़ता है, भ्रष्ट चुनावी प्रथाएं भी सामने आती हैं। हमारे देश में बार-बार होने वाले चुनाव सत्ताधारी दल या राज्य स्तर पर पार्टियों के लिए इस तरह से नीतियां बनाने में सहायक पाए गए हैं ताकि त्वरित राजनीतिक लाभ प्राप्त किया जा सके।
चुनाव से पहले और बाद में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आंतरिक कानून-व्यवस्था और बाहरी सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इससे राष्ट्रीय संसाधनों का भी ह्रास होता है। इन दुष्परिणामों को देखते हुए पिछली सदी के उत्तरार्ध में एक साथ चुनाव कराने के विचार को बल मिला। 1999 में, विधि आयोग ने इस विचार का समर्थन किया और 2018 में, आयोग ने लागत में कटौती और प्रशासनिक बोझ कम करने के उपाय के रूप में इसकी वकालत की।
प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और 2015 से 2019 तक नीति आयोग के सदस्य, बिबेक देबरॉय ने एक चर्चा पत्र तैयार किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, कहा गया कि 30 से अधिक वर्षों में एक भी वर्ष विधानसभा या लोकसभा चुनाव के बिना नहीं रहा। एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता को उचित ठहराने के लिए ऊपर उल्लिखित कुछ नकारात्मक परिणामों पर भी प्रकाश डाला गया।
यह कदम स्वागत योग्य है लेकिन वैचारिक, राजनीतिक, संवैधानिक और परिचालन महत्व वाले कुछ बुनियादी प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं। पाँच अनुच्छेदों – अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 356 में संशोधन करना सबसे बड़ी संवैधानिक चुनौती है क्योंकि इसके लिए न केवल संसद के दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन जुटाना होगा बल्कि आधे से अनुसमर्थन भी करना होगा। राज्य। इस प्रकार, हमें राजनीतिक सर्वसम्मति की आवश्यकता है जो देश के व्यस्त राजनीतिक माहौल को देखते हुए एक दूर का सपना प्रतीत होता है।
संवैधानिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के सवाल को खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि क्या यह ‘बुनियादी ढांचे’ का हिस्सा है, जो केशवानंद भारती मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार संशोधन योग्य नहीं है, यह बहस का मुद्दा हो सकता है। गौरतलब है कि संविधान की मूल संरचना अभी भी एक अपरिभाषित क्षेत्र है।
लागत में कटौती की कवायद के रूप में एक साथ चुनाव एक विवादास्पद प्रस्ताव है क्योंकि इसका कोई अनुभवजन्य प्रमाण नहीं है। इसके अलावा, कोई यह तर्क दे सकता है कि चुनाव कराने में होने वाली लागत आवश्यक रूप से फिजूलखर्ची नहीं है क्योंकि चुनाव के दौरान प्रचार खर्च और आर्थिक गतिविधियों पर कई गुना प्रभाव पड़ता है। दूसरा, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चुनावों को एक साथ कराना लगभग असंभव है। तीसरा, एक साथ चुनाव कराने से साजो-सामान संबंधी व्यवस्था को बड़ी चुनौती मिल सकती है। एक अनुमान के मुताबिक, 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और इतनी ही संख्या में वोटर वेरिफाइड पेपर
credit news: telegraphindia

















