निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार
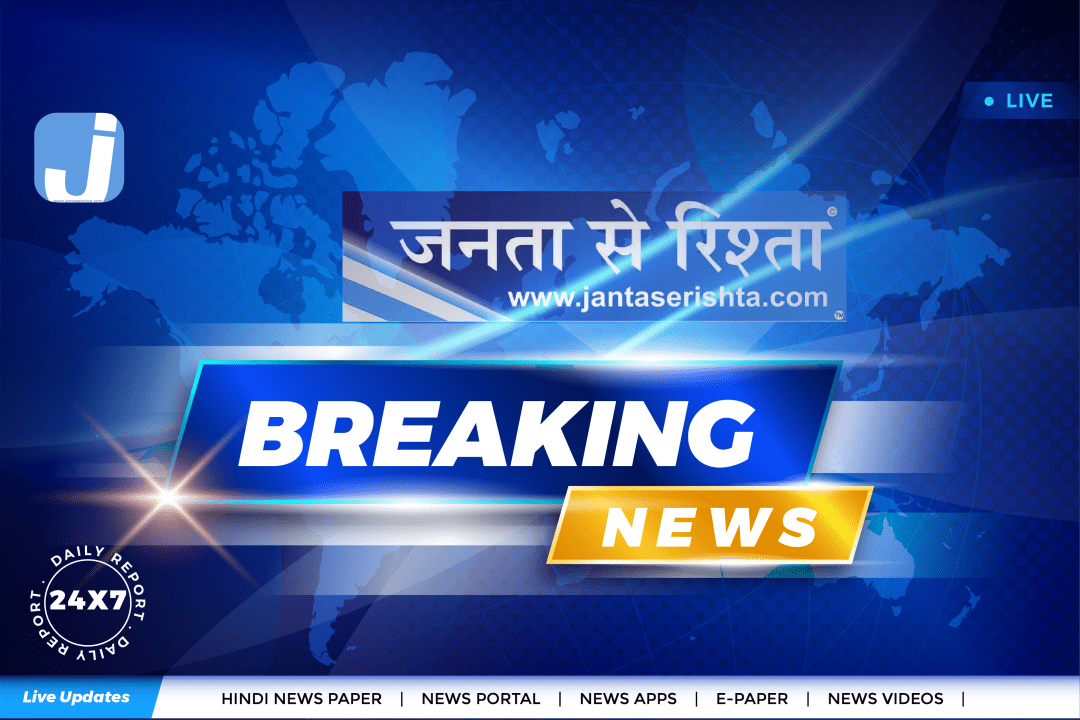
हर साल 9 नवंबर को हम 1995 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम (एलएसए) की शुरुआत को चिह्नित करते हुए राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाते हैं। यह कानून हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है, खासकर अनुच्छेद 39 ए के तहत, जो राज्य पर दायित्व डालता है। निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना।

यद्यपि 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना हमारे संविधान के भीतर एक सिद्धांत है, क्योंकि कानून का शासन स्वयं कानूनी सहायता की पहुंच पर निर्भर करता है। फिर भी, वास्तविक चुनौती गरीबों और कानूनी निरक्षरों के लिए इस आश्वासन को प्रभावी ढंग से लागू करने में है। एनसीआरबी कानूनी सेवा लाभार्थियों की रिपोर्ट (2016-2019) के डेटा से पता चलता है कि केवल 7.91% विचाराधीन कैदियों ने अपनी हकदार कानूनी सहायता सेवाओं का उपयोग किया और लगभग 68% विचाराधीन कैदी निरक्षर हैं, जो सिस्टम की प्रभावशीलता के बारे में चिंताओं को उजागर करता है।
अधिकार का विकास
जबकि अनुच्छेद 39ए को 1976 में एक निदेशक सिद्धांत (डीपीएसपी) के रूप में पेश किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानूनी सहायता न्यायशास्त्र विकसित करने तक इसका प्रभाव सीमित था। एम एच होसकोट केस (1978) में, न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने मेनका गांधी केस (1978) की व्याख्या की और संविधान में अनुच्छेद 21 के बल पर मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार को संचालित किया। उन्होंने निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक कानूनों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस परिवर्तनकारी रुख ने डीपीएसपी से मुफ्त कानूनी सहायता के प्रावधान को प्रभावी ढंग से मौलिक अधिकार में पुनर्वर्गीकृत कर दिया।
इसके बाद, न्यायमूर्ति भगवती ने अपने दो निर्णयों के माध्यम से एक अमिट छाप छोड़ी – हुसैनारा खातून मामले (1979) में, जो बिहार में बिना मुकदमे के वर्षों तक हिरासत में रहने वाले विचाराधीन कैदियों की पीड़ा से संबंधित था, और भागलपुर ब्लाइंडिंग मामले (1981) में। , जहां कानून प्रवर्तन कर्मियों को विचाराधीन कैदियों को तेजाब से अंधा करने के भयानक कृत्य में फंसाया गया था। उन्होंने पुष्टि की कि कानूनी सहायता एक गैर-परक्राम्य आवश्यकता है, और राज्य बजटीय बाधाओं को ढाल के रूप में उपयोग नहीं कर सकता है। परिणामस्वरूप, कानूनी सहायता न्यायिक प्रणाली के मूल ढांचे में अंतर्निहित हो गई।
1977 में, जे अय्यर और जे भगवती की दो सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने एक व्यापक कानूनी सहायता कानून का मसौदा प्रस्तावित किया। 1980 में, कानूनी सहायता योजनाओं को लागू करने के लिए समिति (CILAS) को एक राष्ट्रव्यापी मॉडल कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था, जिससे सभी राज्यों में कानूनी सहायता बोर्डों का गठन हुआ। बाद में, 1987 में विभिन्न स्तरों पर कानूनी सेवा प्राधिकरणों के निर्माण को अनिवार्य करते हुए कानूनी सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम लागू किया गया।
हाल ही में 2022 में, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने अभूतपूर्व कानूनी सहायता रक्षा परामर्श योजना (एलएडीसीएस) की शुरुआत की, जहां सार्वजनिक रक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में पुलिस हिरासत में व्यक्तियों और आपराधिक मामलों में प्रतिवादियों को मुफ्त कानूनी सहायता की पेशकश की जाएगी। सरकारी अभियोजकों के समान समर्पित वकीलों की एक टीम को एक निश्चित मासिक वेतन पर नियुक्त किया जाएगा और विशेष रूप से इन मामलों को संभाला जाएगा। यदि पूरी तरह से क्रियान्वित किया जाता है, तो यह कार्यक्रम विचाराधीन बंदियों और आपराधिक मामलों में निर्धन प्रतिवादियों को महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित कर सकता है।
इसमें क्या शामिल है
कानूनी सहायता न केवल राज्य का कर्तव्य है, बल्कि अभियुक्तों का अधिकार भी है, यहाँ तक कि अजमल कसाब से जुड़े मुंबई हमलों जैसे जघन्य मामलों में भी। सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट है कि सुनवाई शुरू होने पर वकील उपलब्ध कराने में विफलता पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसमें आपराधिक, नागरिक और प्रशासनिक मामलों में कानूनी प्रतिनिधित्व के साथ-साथ वंचित व्यक्तियों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना शामिल है। यह महिलाओं, एसटी और एससी, विकलांग व्यक्तियों, आपदा पीड़ितों और मानव तस्करी से बचे लोगों जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों की सहायता करता है। कानूनी सहायता में जनहित याचिका, सामाजिक-कानूनी सर्वेक्षण करना, अदालती खर्चों को कवर करना, दस्तावेज़ पुनर्प्राप्ति और पात्र प्राप्तकर्ताओं के लिए अपील की तैयारी भी शामिल है।
बाधाएँ, सफलताएँ
कानूनी सहायता से संबंधित उल्लेखनीय मुद्दों में से एक कानूनी सहायता परामर्शदाताओं (एलएसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में निहित है। कई उदाहरणों में, व्यक्ति केवल अंतिम उपाय के रूप में कानूनी सहायता की ओर रुख करते हैं, अक्सर निजी कानूनी सेवाओं को प्राथमिकता देते हैं। कानूनी सहायता क्लीनिकों की रीब्रांडिंग की सख्त जरूरत है। यह बेहतर धारणा विश्वास को बढ़ावा देती है, जो लाभार्थी की संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण है, अंततः कानूनी सहायता आंदोलन को मजबूत करती है।
लेकिन, एलएसी को कम मानदेय और विलंबित भुगतान की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, अपर्याप्त संसाधन, जैसे पुस्तकालय और बैठक स्थान स्थिति को और खराब कर देते हैं। चुनिंदा भारतीय जिलों में एलएडीसीएस की शुरूआत इन समस्याओं का समाधान प्रदान करती प्रतीत होती है। हालाँकि, कई और क्षेत्रों को शामिल करने के लिए तेजी से विस्तार की आवश्यकता है। एक अन्य मुद्दा सक्षम एलएसी को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया से संबंधित है, क्योंकि यह आम तौर पर सेवा की गुणवत्ता पर वर्षों के अभ्यास को प्राथमिकता देता है, इस प्रकार समावेशन के लिए एक मानकीकृत उपाय का अभाव होता है। उदाहरण के लिए, जैसा कि मोहम्मद हुसैन मामले (2012) में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नियुक्त एलएसी गवाहों के सामने आने और यहां तक कि उनसे जिरह करने में भी विफल रही। जबकि एलएडीसीएस ने आपराधिक मामलों में अधिवक्ताओं के लिए विशिष्ट मानक मानदंड निर्धारित किए हैं परीक्षणों में, इस मानकीकरण को अन्य प्रकार के मामलों में विस्तारित करने की समान आवश्यकता है।
वर्तमान कानूनी सहायता वार्ता गैर-वकीलों को न्यायाधिकरणों और आयोगों में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देकर कानूनी सेवाओं की पहुंच को व्यापक बनाने पर विचार करती है। दिलचस्प बात यह है कि 1961 का अधिवक्ता अधिनियम अधिवक्ताओं को पढ़ाने की अनुमति देता है, जबकि कई पंजीकृत अधिवक्ता होने के बावजूद, कानून शिक्षकों के लिए यह पारस्परिक नहीं है। कानून शिक्षकों को सीमित अभ्यास विशेषाधिकार देने से कानूनी सहायता में सुधार हो सकता है। फिर भी, कानूनी सहायता क्लीनिकों के माध्यम से कुछ नि:शुल्क मामलों को अनिवार्य रूप से लेने के लिए कानूनी पेशेवरों को विनियमित करना एक प्रभावी रणनीति है।
प्रौद्योगिकी और आभासी अभ्यास का विस्तारित उपयोग, विशेष रूप से निचली अदालतों में, वकीलों को दूर-दराज के क्षेत्रों से भी कई प्रो-बोनो मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देगा। इससे मुकदमेबाजी में देरी और लागत दोनों में काफी कमी आएगी। इसके अलावा, कानून के छात्र की भूमिका को पहचानना आवश्यक है। समग्र नैदानिक कानूनी शिक्षा को एकीकृत करना न केवल उन्हें सामाजिक-कानूनी मुद्दों को समझने में सक्षम बनाता है, बल्कि उन व्यक्तियों की सहायता करने में भी सक्षम बनाता है जिनके पास कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंच नहीं है।
अंत में, ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 को उद्देश्य के अनुसार क्रियान्वित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक आशाजनक नीति है जिसे लागू नहीं किया गया है। यह कदम विशेष रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय तक त्वरित पहुंच की गारंटी देगा। किसी को यह समझना चाहिए कि कानूनी सहायता न केवल स्वतंत्रता की रक्षा करती है बल्कि गरिमा को भी बरकरार रखती है और गरीबी के खिलाफ एक कवच के रूप में कार्य करती है।
Prof Dr GB Reddy, Pavan Kasturi
Telangana Today

















