बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची आने में देरी होगी
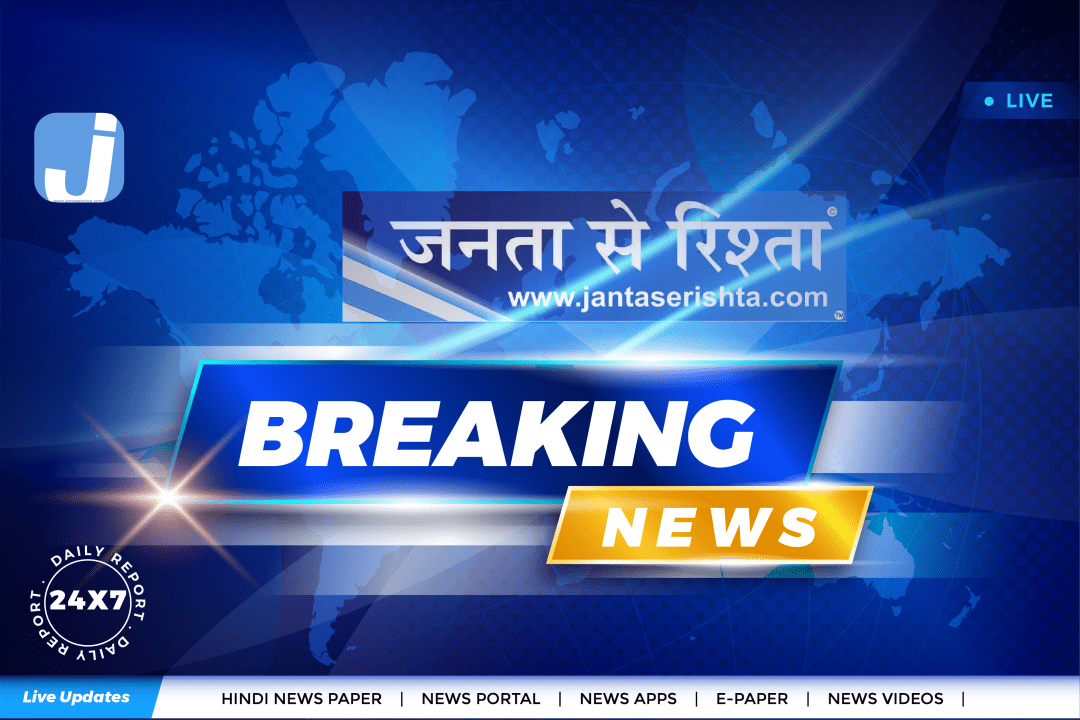
हैदराबाद: भले ही भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए दावेदारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक बैठक आयोजित करने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है कि पैनल जल्द ही तेलंगाना के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगा।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक ऐसा इसलिए क्योंकि कमेटी पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवार तय कर रही है. सूत्रों ने टीएनआईई को बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ कोई स्पष्टीकरण देने के लिए समिति की बैठक में शामिल हो सकते हैं। चूंकि किशन रेड्डी के 17 अक्टूबर तक नई दिल्ली जाने की उम्मीद नहीं है, इसलिए पार्टी नेताओं का कहना है कि 38 नामों वाली पहली सूची जारी होने में देरी हो सकती है, जिसके 16 अक्टूबर को जारी होने की उम्मीद थी।
फिलहाल स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों पर काम कर रही है और अभ्यास के बाद सीईसी को नामों की सिफारिश करेगी। सूत्रों ने कहा कि 2024 में लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों को भी आगामी चुनावों में अपनी योग्यता साबित करनी होगी।
उम्मीदवारों की पहली सूची उन निर्वाचन क्षेत्रों से आएगी जहां उम्मीदवारों को लेकर आम सहमति है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “पार्टी के केंद्रीय और राज्य नेताओं द्वारा व्यापक परामर्श के अलावा, हम उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने से पहले सर्वेक्षणों के परिणामों और उम्मीदवारों की संभावनाओं को ध्यान में रखेंगे।”

















