हाईवे पर हुआ भारी भूस्खलन, मलबे की चपेट में आई कार
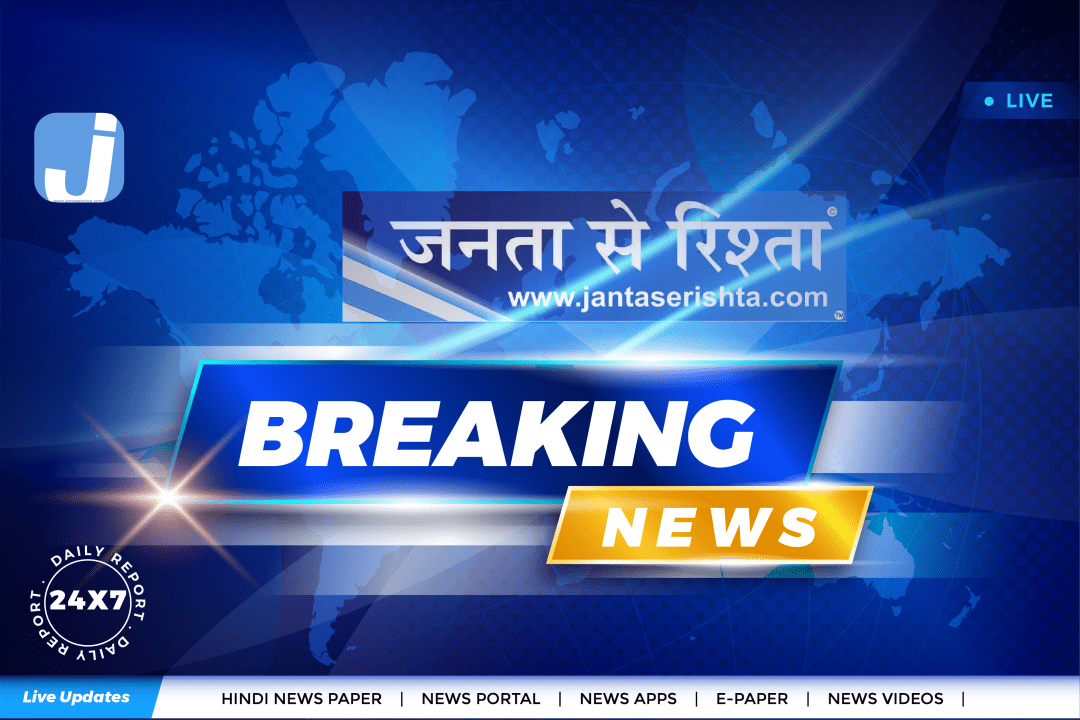
मंडी। जिला मंडी में सुंदरनगर-करसोग हाईवे पर भग्यार के समीप भूस्खलन हो गया है। वहीं भूस्खलन के चलते मलबे की चपेट में कार भी आ गई है। कार सवार दो लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।
वहीं मार्ग बंद होने से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क मार्ग बंद होने से दोनों ओर जाम की स्थिति पैदा हो गई है और लोगों को वैकल्पिक मार्ग के माध्यम से सफर करना पड़ रहा है।
मामले की पुष्टि करते हुए उपमंडल अधिकारी सुंदरनगर अमर नेगी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की टीम ने मार्ग बहाली का कार्य शुरू किया है। उन्होंने बताया कि मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए जल्दी बहाल कर दिया जाएगा।














